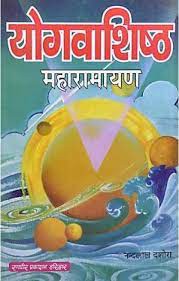
योगवासिष्ठ ग्रन्थ वसिष्ठ-रामायण, महारामायण आदि नामों से भारत ही नहीं विश्व साहित्य जगत में विख्यात है। भगवान् श्रीराम को ज्ञानस्वरूप महर्षि वसिष्ठ ने उन्हें तत्वज्ञान की इस ग्रन्थ में शिक्षा दी है। इस ग्रन्थ में जीव-जगत, बन्धन-मोक्ष, आत्मा-परमात्मा आदि दुरुह विषयों का अनेक दृष्टान्तों और कथानकों के द्वारा बड़ा ही सुन्दर-सरल विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ के विषय में महर्षि-वसिष्ठजी ने स्वयं कहा है कि संसार सर्प के विष से विकल तथा विषय-विषूचिका से पीड़ित प्राणियों के लिए योगवासिष्ठ श्रेष्ठ परम पवित्र अमोघ ग्रन्थ है। इसमें बताया गया है कि अहंकार का नाश होते ही केवल एक ब्रह्म चैतन्य ही रह जाता है। मानव जीवन में सदाचार और सत्संग की महत्ता का उदाहरण इस ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर प्रतिपादन किया है।
ईश्वर प्रदत्त जीवन जीने के लिए इस लेख में महर्षि वसिष्ठजी ने श्रीराम को इच्छा के बन्धन, इच्छा के त्याग के द्वारा मुक्ति का मार्ग समझाया है। महर्षि वसिष्ठ कहते हैं- हे रघुकुल भूषण राम! इस संसार में जितने भी अनर्थस्वरूप सांसारिक पदार्थ है, वे सभी जल में आवर्तकी भाँति भिन्न-भिन्न रूप धारण करके चमत्कार उत्पन्न करते हैं अर्थात् इच्छाओं को उत्पन्न करके चित्त को माया-मोह के जाल में फँसा देते हैं किन्तु जैसे सभी लहरें जलस्वरूप ही हैं, वैसे ही सम्पूर्ण पदार्थ वस्तुत: नश्वर स्वभाव (प्रकृति) के हैं। उदाहरणस्वरूप जैसे बालक की चिन्ता से कल्पित यक्ष-पिशाच आदि का रूप उसके समान ही आकाश में दीख पड़ता है किन्तु मुझ जैसे ज्ञानी के लिए वह कुछ भी नहीं है। उसी तरह मेरी दृष्टि में तत्तत्व: यह विश्व कुछ भी नहीं है, किन्तु अज्ञानी के चित्त में यही सत्य सा सदैव प्रतीत होता है। यह विश्व पत्थर पर खुदी हुई पुतलियों की सेना की भाँति रूपालोक तथा बाह्य और अभ्यन्तर विषय से शून्य है। फिर क्यों इसमें विश्वता कैसी? किन्तु अज्ञानियों के लिए यह रूपालोक और मनन आदि से युक्त प्रतीत होता है। श्रीराम! इस जगत् को जगद्रूप से जानना भ्रम है और इसे जगद्रूप न जानना भ्रमशून्यता है। श्रीराम! त्वत्ता और अहंता आदि सारे विभ्रम-विलास शान्त, शिव तथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप ही है, इसलिए मुझे ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता- ठीक वैसे ही जैसे आकाश में कानन कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होता है।
श्रीराम! जिसकी चेष्टा प्रारब्ध प्राप्त कर्मों में कठपुतली की तरह इच्छा शून्य तथा व्याकुलता रहित होती है, वहीं विश्रान्त मनवाला जीवन्मुक्त मुनि है। जीवन्मुक्त ज्ञानी को इस जगत् का जीवन बांस की तरह बाहर-भीतर से शून्य रसहीन और वासनारहित प्रतीत होता है। जिसकी इस दृश्य-प्रपञ्च में रुचि नहीं है और हृदय जिसे चिन्मात्र अदृश्य ब्रह्म ही श्रेष्ठ अच्छा लगता है, उसने मानो बाहर-भीतर से शान्ति प्राप्त कर ली और वह इस भवसागर से पार हो गया।
हे रघुनन्दन! शास्त्रज्ञों के मतानुसार मन का इच्छारहित हो जाना ही समाधि की अवस्था है क्योंकि मन को जैसी शान्ति इच्छा का त्याग कर देने से प्राप्त होती है वैसी सैकड़ों उपदेशों से भी उपलब्ध नहीं होती। इच्छाओं की उत्पत्ति से जैसा दु:ख प्राप्त होता है, वैसा दु:ख तो नरक में भी नहीं मिलता है और इच्छा की शान्ति जैसा सुख मिलता है वैसे सुख का अनुभव तो ब्रह्म लोक में भी नहीं होता है। इसीलिए समस्त तपस्याओं, यमों, शास्त्रों और नियमों का पर्यवसान इतने में ही है कि इच्छा मात्र को ही दु:खदायक चित्त कहते हैं तथा उस इच्छा की शान्ति ही मोक्ष कहलाता है। किसी भी प्राणी के हृदय में जैसी-जैसी और जितनी-जितनी इच्छा उत्पन्न होती है, उतनी-उतनी ही उसके दु:खों के बीजों की मूँठ बढ़ती जाती है। विवेक विचार द्वारा जैसे-जैसे उसकी इच्छा क्षीण होती जाती है, वैसे-वैसे ही उसके दु:खों की चिन्तारूपी विषूचिका शान्त होती जाती है। सांसारिक विषयों की इच्छा आसक्तिवश ज्यों-ज्यों घनीभूत होती जाती है त्यों-त्यों दु:खों की चिन्तारूपी विषैली तरंगे बढ़ती जाती है। यदि अपने पौरुष-प्रयत्न बल से इस इच्छा व्याधि की चिकित्सा न हो सकी तो मैं यह दृढ़तापूर्वक समझता हूँ कि इस व्याधि से छूटने के लिए दूसरी कोई औषधि है ही नहीं। यदि एक ही साथ सम्पूर्ण इच्छाओं का पूर्णतया त्याग न किया जा सके तो धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके ही उसका त्याग करना चाहिए। सन्मार्ग का पथिक कभी भी दु:खभागी नहीं होता है। जो नराधम अपनी इच्छाओं के क्षीण करने का प्रयत्न नहीं करता है वह मानों दिन पर दिन अपने आपको अन्धकूप में फेंक रहा है। इच्छा ही दु:खों को जन्म देने वाली इस संसृति रूपी बेल का बीज है। यदि आप उसे आत्मज्ञानरूपी अग्नि से ठीक प्रकार से जला दें तो यह पुन: अंकुरित नहीं होता है।
हे रघुकुल भूषण राम! आखिर इच्छा है क्या? इच्छा मात्र ही संसार है और इच्छा का अवेदन-अभाव ही निर्वाण है। इसलिए निरर्थक नाना प्रकार के उलट फेर में न पड़कर केवल ऐसा यत्न करना चाहिए कि इच्छा उत्पन्न ही न हो। जिसे अपनी बुद्धि से इच्छा का विनाश करना दुस्साध्य प्रतीत होता हो, उसके लिए गुरु का उपदेश और शास्त्र आदि निश्चय ही निरर्थक है। जैसे अपनी जन्मभूमि जंगल में हरिणी की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही नानाविध दु:खों का विस्तार करने वाली इच्छारूपी विष के विकार से युक्त इस जगत् में मनुष्यों की मृत्यु बिलकुल निश्चित है। यदि मनुष्य इच्छा द्वारा बालकों-जैसा मूढ़ न बना दिया जाए तो उसे आत्मज्ञान के लिए बहुत थोड़ा ही प्रयत्न करना पड़े। इसलिए सब तरह से इच्छा को ही शान्त करना चाहिए, क्योंकि उसकी शान्ति से ही परमपद की प्राप्ति होती है। इच्छारहित हो जाना ही निर्वाण है तथा इच्छायुक्त होना ही बन्धन है, इसलिए यथाशक्ति इच्छा पर विजय प्राप्त कर जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। बस इतना करने में कौन सी कठिनाई है? जन्म जरा और मृत्यु रूप करञ्ज और खैर के वृक्ष-समूहों का बीज इच्छा ही है अत: उसे शमरूपी अग्रि से सदा भीतर ही भीतर जला डालना चाहिए। जहाँ-जहाँ इच्छा का सम्बन्ध है, वहाँ-वहाँ पुण्य-पापमयी दु:खराशियों तथा विस्तृत पीड़ाओं से युक्त बन्धनपाशों को उपस्थित ही समझना चाहिए। ज्यों-ज्यों पुरुष की आन्तरिक इच्छा शान्त होती जाती है, त्यों-त्यों उसका मोक्ष के लिए कल्याणकारक साधन बढ़ता जाता है। विवेकहीन आत्मा की इच्छा को जो भलीभाँति पूर्ण करना है, वही मानों संसाररूपी विष वृक्ष को सींचना है।
इस संसार सागर में सदा इच्छा, माया और मोह से विरक्त होना चाहिए यथा-
मम माता मम पिता मम भार्या ममात्मजा:।
ममेदमिति जन्तूनां ममता बाधते वृथा।।
(वाल्मीकि रामायण माह ४-२६)
मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा घर, इस प्रकार ममता (आसक्ति) प्राणियों को व्यर्थ में ही सताती रहती है।
सन्दर्भ ग्रन्थ-
१. योग-वासिष्ठ
२. वाल्मीकि रामायण
(लेखक- डॉ. नरेन्द्रकुमार मेहता )


.jpg)

